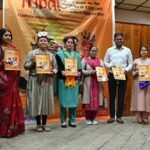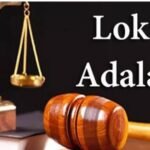सुरभि न्यूज़
डॉ सत्यवान सौरभ, हिसार : हरियाणा
जब लोकतंत्र का प्रहरी संपादक, जनता से संवाद बंद कर दे और सत्ता का दरबारी बन जाए, तब पत्रकारिता दम तोड़ने लगती है। आज बड़े संपादक आम आदमी से कट चुके हैं, गाँव-कस्बों की आवाज़ें अखबारों में गुम हैं। संवाद की जगह प्रचार ने ले ली है। सत्ता और पूँजी के एजेंडे चलाए जा रहे हैं। अब वक्त है संपादकों को चौपाल में वापस लाने का, जहाँ हर नागरिक का सवाल सुना जाए और जवाबदेही तय हो। वरना लोकतंत्र महज़ एक सजावटी तमाशा बनकर रह जाएगा।
भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान के पहले शब्द ही कहते हैं—”हम भारत के लोग…”। यानी इस देश में हर पद, हर संस्था, हर कानून की जड़ें जनता में हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के सबसे ज़रूरी स्तंभ—मीडिया—और उसमें भी सबसे असरदार वर्ग—संपादक—ही जनता से मुंह मोड़ ले, तो सवाल उठाना लाज़मी हो जाता है।
आजकल बड़े-बड़े अखबारों के कई संपादक आम आदमी से बात तक नहीं करते। कॉल रिसीव करना तो दूर, उनका अंदाज़ ऐसा होता है जैसे जनता से बात करना उनकी शान के ख़िलाफ़ है। जिनका काम था जनता की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक ले जाना, वो खुद सत्ता की चुप्पी के दरबारी बन बैठे हैं। ऐसे में ये पूछना ज़रूरी है कि इन ‘महाराजा संपादकों’ की हमारे लोकतंत्र में भूमिका क्या है?
कभी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। लेकिन अब यह स्तंभ कॉरपोरेट की छत पर खड़ा नज़र आता है। गाँव का किसान, छोटी दुकान चलाने वाला, दिहाड़ी मज़दूर, बेरोज़गार युवा—इनकी खबरें अब ना टीवी के प्राइम टाइम में आती हैं, ना अखबारों के कॉलम में। क्योंकि ये न टीआरपी लाते हैं, न विज्ञापन। आज का संपादक जनता की नब्ज़ नहीं, सत्ता और पूँजी की धड़कन देख रहा है। इस डर से कि कहीं विज्ञापन की सांसें न थम जाएं।
संपादक अब संवाद नहीं करते, वो आदेश देते हैं। वे खुद तय करते हैं कि कौन सी खबर छपेगी, कौन सा मुद्दा दिखेगा और कौन सा दबा दिया जाएगा। हरियाणा से बंगाल तक, मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र तक हज़ारों आंदोलन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बड़े अखबारों में उनकी एक लाइन नहीं छपती। संपादक अब यह नहीं सोचते कि जनता क्या जानना चाहती है, वे ये सोचते हैं कि सरकार और उद्योगपतियों को क्या दिखाना है।
ये कैसी विडंबना है कि जिस देश में राष्ट्रपति तक को कोई भी नागरिक पत्र लिख सकता है, प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ के ज़रिए जनता से सीधे संवाद करता है, वहां एक अखबार का संपादक आम आदमी के ईमेल को भी समय की बर्बादी समझता है। जब संवाद का माध्यम ही ‘selective hearing’ करने लगे, तो लोकतंत्र बहरा होने लगता है।
जब संपादक जनता की बात नहीं सुनते, तो फिर वे किसके लिए लिखते हैं? उत्तर साफ़ है—सरकार और पूँजी के लिए। अब अखबार सूचना का माध्यम नहीं रहे, वे इमेज मैनेजमेंट के औज़ार बन चुके हैं। हर दिन पहले से तय होता है कि किन नेताओं की छवि चमकानी है, किस उद्योगपति को हीरो बनाना है, और किन जन आंदोलनों को अनदेखा करना है।
अब पत्रकारिता नहीं, प्रचार है। कुछ संपादक अब पत्रकार नहीं, बल्कि सत्ताधारी दलों के प्रवक्ता लगते हैं। उनकी भाषा, उनकी हेडलाइंस, उनका विश्लेषण—सबमें एक खास झुकाव झलकता है और ये झुकाव विचारधारा का नहीं, विज्ञापन और पहुंच का है। वो कहावत थी ना—“इतना मत डराओ कि कोई सच बोलना ही छोड़ दे।” पर आज तो संपादक खुद ही सत्ता से डरते हैं और जनता से कतराते हैं।
देश की आधी आबादी अब भी गाँवों में रहती है। लेकिन गाँवों की समस्याएं—बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, दलितों पर अत्याचार, खेती का संकट—बड़े अखबारों के लिए मानो अस्तित्वहीन हैं। जब तक कोई हादसा आत्महत्या या गैंगरेप न बन जाए, तब तक उसकी खबर नहीं बनती। क्या मीडिया ने तय कर लिया है कि बस महानगरों की संवेदनाएं ही ‘खबर’ हैं?
इस पूरे परिदृश्य में एक बात बहुत स्पष्ट है—अगर पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो संपादकों को ‘महाराजा’ बनना छोड़ना होगा। उन्हें फिर से जनता का सेवक बनना होगा। दरबार नहीं, चौपाल सजानी होगी। संपादक अगर आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर सुनेगा कौन? अगर मीडिया ही गूंगा हो जाए, तो लोकतंत्र खुद बहरा हो जाता है।
अब ज़रूरी है कुछ बुनियादी सवाल उठाना :
क्या बड़े मीडिया घरानों को RTI के दायरे में लाया जाए?
क्या संपादकों की जवाबदेही तय की जाए?
क्या संपादकों को भी जनसुनवाई के लिए बाध्य किया जाए?
क्या स्वतंत्र पत्रकारों और छोटे अखबारों को विज्ञापन में प्राथमिकता दी जाए?
जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिलते, तब तक संपादक नामक पद लोकतंत्र के भीतर बैठा एक लघु तानाशाह ही रहेगा।
संपादक जनता का एक प्रतिनिधि होता है, उसकी कलम जनता के आंसुओं से स्याही खींचती है। अगर वह कलम अब सत्ता की जेब में रखी रहने लगी है, तो समझिए कि शब्द बिक चुके हैं, विचार गिरवी रखे जा चुके हैं, और जनता अब सिर्फ पाठक नहीं, बल्कि शोषित बन चुकी है।
आज ज़रूरत है इन महाराजा संपादकों का पर्दाफाश करने की। पत्रकारिता को फिर से चौपाल में लाने की। हर आम नागरिक को यह हक़ होना चाहिए कि वो सवाल पूछ सके, और उसे जवाब मिले। वरना लोकतंत्र एक रंगमंच बनकर रह जाएगा। जहाँ नायक भी बिके हुए होंगे, और संवाद भी पहले से लिखे हुए। सच्चा लोकतंत्र वही होता है, जहाँ एक किसान भी संपादक को चिट्ठी लिख सके, और उसे उत्तर मिले।
लेखक कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट है।